नया प्रतिजैविक : टीक्सोबैक्टिन
प्रेमचंद्र श्रीवास्तव
 ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेसली ऑरगेल सदैव यह मानते थे कि विकास (इवोल्यूशन) की प्रक्रिया मानवीय बुद्धि कौशल की तुलना में अधिक चालाक है। शनैः शनैः बारंबार प्रतिजैविकों के लिए प्रतिरोधी जीवाणुओं के विकास ने इस बात को सही भी सिद्ध किया है। जब 1940 के दशक में वैज्ञानिकों ने मनुष्यों के लिए प्रतिजैविकों का निर्माण प्रारंभ किया था तभी से धीरे-धीरे जीवाणुओं ने भी प्रतिजैविकों के प्रति अपने भीतर मानवीय प्रयासों के विरुद्ध प्रतिरोधिता विकसित करने की आदत सी डाल ली थी। आज यह स्थिति आ गई है कि वे जीत की ओर अग्रसर हैं। जीवाणुओं ने ऐसे उपभेद (स्ट्रेन्स) विकसित कर लिए हैं जिनमें अपने पुराने शत्रु प्रतिजैविकों के लिए भारी प्रतिरोधक्षमता उत्पन्न हो गई है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे हथियार उनके आगे अक्षम सिद्ध होने लगे हैं।
ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक लेसली ऑरगेल सदैव यह मानते थे कि विकास (इवोल्यूशन) की प्रक्रिया मानवीय बुद्धि कौशल की तुलना में अधिक चालाक है। शनैः शनैः बारंबार प्रतिजैविकों के लिए प्रतिरोधी जीवाणुओं के विकास ने इस बात को सही भी सिद्ध किया है। जब 1940 के दशक में वैज्ञानिकों ने मनुष्यों के लिए प्रतिजैविकों का निर्माण प्रारंभ किया था तभी से धीरे-धीरे जीवाणुओं ने भी प्रतिजैविकों के प्रति अपने भीतर मानवीय प्रयासों के विरुद्ध प्रतिरोधिता विकसित करने की आदत सी डाल ली थी। आज यह स्थिति आ गई है कि वे जीत की ओर अग्रसर हैं। जीवाणुओं ने ऐसे उपभेद (स्ट्रेन्स) विकसित कर लिए हैं जिनमें अपने पुराने शत्रु प्रतिजैविकों के लिए भारी प्रतिरोधक्षमता उत्पन्न हो गई है। दुर्भाग्य यह है कि हमारे हथियार उनके आगे अक्षम सिद्ध होने लगे हैं।
नवीनतम सूचना के अनुसार 1962 के पूर्व ही विज्ञानियों ने बीस से अधिक नए प्रतिजैविकों का निर्माण कर लिया था। उसके पश्चात् अब तक केवल दो ही और महत्वपूर्ण प्रतिजैविकों का विकास किया जा सका है। हाल ही में बोस्टन, मैसाचुसेट्स की नार्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी से सम्बद्ध किम लेविस के नेतृत्व में उनके शोधार्थियों के दल ने एक नए प्रतिजैविक टीक्सोबैक्टिन की पहचान करके इस दिशा में एक नई उपलब्धि हासिल की है। यह प्रतिजैविक कुछ प्रकार के जीवाणुओं के बाह्य आवरण के निर्माण को बाधित करके उन्हें नष्ट कर डालते हैं। टीक्सोबैक्टिन दशकों में घोषित किया जाने वाला पहला नया प्रतिजैविक है। यह प्रतिजैविक उन रोगजनक ग्राम पॉजिटिव जीवाण्ुाओं के विरुद्ध सक्रिय होता है जिन्होंने उपलब्ध स्वीकृत प्रतिजैविकों के विरुद्ध प्रतिरोधकता विकसित कर ली है। इस खोज की सूचना सन 2015 के जनवरी माह में प्रकाशित हुई। शोधार्थियों द्वारा विकसित की गई एक नई तकनीक से इस प्रतिजैविक को स्वस्थाने (उसके प्राकृतिक निवास में ) असंवर्धित जीवाणुओं के एक परीक्षण में खोज निकाला गया। जिस उल्लेखनीय पद्धति से इसकी खोज की गई है उसके कारण यह सूचना और भी महत्वपूर्ण हो गई है। वस्तुतः पिछले कुछ दशकों से प्रतिजैविकों के निर्माण की ओर औषधि कम्पनियों की रुचि समाप्त सी हो गई थी क्योंकि कम्पनियों का ध्यान अधिक लाभ देेने वाली औषधियों के प्रति आकर्षित हो गया था। अधिकांश कम्पनियाँ मधुमेह या हृदय रोग जैसे दीर्घकालिक रोगों की औषधियों के निर्माण की ओर अधिक संलग्न होने लगी थीं तथा प्रतिजैविक औषधियों को कम महत्वपूर्ण मानकर (आर्थिक दृष्टि से) उनके साथ सौतेला व्यवहार होने लगा था।
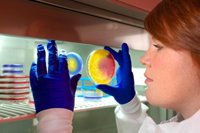 जब जनवरी 2015 में अमेरिका और जर्मनी के चार शोध संस्थानों और दो औषधि कम्पनियों ने सूचना दी कि उन्होंने एक नया प्रतिजैविक खोज लिया है तो चिकित्सा जगत में उत्तेजना व्याप्त हो गई। इसके आविष्कर्ताओं द्वारा यह भी दावा किया गया था कि इसमें इतनी मारक क्षमता है कि इसके विरुद्ध कोई भी प्रतिरोध होता नहीं दिखाई पड़ता। आई चिप ; प् बीपचद्ध तकनीक का इस्तेमाल करते हुए असंवर्धनीय मृदा जीवाणुओं के परीक्षण के लिए टीक्सोबैक्टिन को पूर्व में असंवर्धित इलेफ्थेरिया टेरी ;म्समजिीमतपं जमततंमद्ध से खोज निकाला गया था । बोस्टन के नार्थ ईस्टर्न विश्वविद्यालय के डॉ. किम लेविस और स्लावा एप्सटीन के अनुसार 99ः जीवाणुओं को हमारी आज की उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीक से वर्धित नहीं कराया जा सकता। इसके लिए उन्होंने एक नई तकनीक ढूंढ़ निकाली है जिसे उन्होंने आई चिप
जब जनवरी 2015 में अमेरिका और जर्मनी के चार शोध संस्थानों और दो औषधि कम्पनियों ने सूचना दी कि उन्होंने एक नया प्रतिजैविक खोज लिया है तो चिकित्सा जगत में उत्तेजना व्याप्त हो गई। इसके आविष्कर्ताओं द्वारा यह भी दावा किया गया था कि इसमें इतनी मारक क्षमता है कि इसके विरुद्ध कोई भी प्रतिरोध होता नहीं दिखाई पड़ता। आई चिप ; प् बीपचद्ध तकनीक का इस्तेमाल करते हुए असंवर्धनीय मृदा जीवाणुओं के परीक्षण के लिए टीक्सोबैक्टिन को पूर्व में असंवर्धित इलेफ्थेरिया टेरी ;म्समजिीमतपं जमततंमद्ध से खोज निकाला गया था । बोस्टन के नार्थ ईस्टर्न विश्वविद्यालय के डॉ. किम लेविस और स्लावा एप्सटीन के अनुसार 99ः जीवाणुओं को हमारी आज की उपलब्ध प्रयोगशाला तकनीक से वर्धित नहीं कराया जा सकता। इसके लिए उन्होंने एक नई तकनीक ढूंढ़ निकाली है जिसे उन्होंने आई चिप
;प् बीपचद्ध तकनीक का नाम दिया है। शोधार्थियों ने टीक्सोबैक्टिन का सफल प्रयोग चुहियों में प्रतिजैविक प्रतिरोधी संक्रमणों की चिकित्सा हेतु किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि जब उन्होंने प्रयास करके जीवाणुओं के औषधि के प्रति प्रतिरोध दर्शाने वाले उपभेदों को विकसित करना चाहा तो वे असफल रहे। ऐसा प्रतीत होता है कि टीक्सोबैक्टिन ‘प्रतिरोध के प्रति ही प्रतिरोधी’ है। रसायनविद लेसली ऑर्गल ने अवश्य थोड़ी आशंका व्यक्त की है कि जीवाणु अंत में टीक्सोबैक्टिन के प्रति भी प्रतिरोधिता विकसित कर लेंगे। किन्तु अन्य शोधार्थी आशावान है कि ऐसा होने में वर्षों नहीं दशकों का समय लग जायेगा । तब तक नए प्रतिजैविकों की खोज के लिए वैज्ञानिकों को पर्याप्त समय मिल जायेगा। उल्लेखनीय बात यह है कि शोध की इस कथा का प्रमुख पात्र और महानायक यह टीक्सोबैक्टिन ही नहीं है। इस सम्मान का सेहरा बँधता है उस आई चिप उपकरण पर जिसका उपयोग करके शोधदल ने इस विशेष यौगिक को ढँूढ़ निकाला है। दूसरे शब्दों में कहें तो टीक्सोबैक्टिन एक मछली है और आई चिप मछली पकड़ने वाली डंडी, जिससे ‘मछली’ को पकड़ना संभव हो सका। इस ‘फिशिंग रॉड’ का पास में होना ही यह सुनिश्चित करता है कि हमें इसकी सहायता से अधिकाधिक ‘मछलियाँॅ’ (दूसरे शब्दों में नए प्रतिजैविक) मिल सकेंगी और सच पूछिए तो हमें और अधिक की आवश्यकता भी है। हमारे इस धरती पर अस्तित्व में आने के खरबों वर्ष पूर्व (बिलियन वर्ष पूर्व) से ही जीवाणु एक दूसरे से युद्धरत थे। इन्हीं में मानवता के लिए लाभकारी और घातक दोनों प्रकार के जीवाणु सम्मिलित थे। अतः ये पर्यावरणीय सूक्ष्मजीव ही प्रतिजैविकों के संभावित प्रचुर स्रोत बन सके। समस्या यह है कि जैसा पहले ही उल्लेख किया गया 99ः जीवाणु प्रयोगशालाओं की दशाओं में वृद्धि नहीं करते हैं। इसलिए शोधकर्मियों ने प्रयास किया कि पर्यावरण की परिस्थितियों को ही प्रयोगशाला में उपस्थित कर दिया जाये। टीक्सोबैक्टिन प्रतिजैविक की खोज में जिस आई चिप की चर्चा की गई है वह यही कार्य करता है।
यह उपकरण एक प्रकार का फलक (बोर्ड) है जिसमें बहुत से छिद्र होते हैं। प्रयोग के लिए शोधदल ने मिट्टी वहीं से प्राप्त की जहाँ वह जीवाणु प्राकृतिक रूप से मिट्टी में पाये जाते हैं। मिट्टी के इस नमूने को पानी में डालकर तनुकृत किया जाता है। फिर इसे खूब हिलाया जाता है जिससे उसमें स्थित सूक्ष्मजीव मिट्टी से अलग हो जायें । पुनः इसमें और जल मिलाकर इसे और तनुकृत किया जाता है। अब इस घोल में द्रवीभूत ‘अगर’ ;ंहंतद्ध को मिलाकर आई चिप बोर्ड के छिद्रों में भर दिया जाता है। अत्यधिक तनुकृत घोल होेने के कारण यह सुनिश्चित हो जाता है कि जमने के बाद हर छिद्र में ठोस हो गई ‘अगर’ की डिस्क में केवल एक जीवाणु कोशिका ही विद्यमान होगी। इस प्रक्रिया के बाद इन डिस्कों को पारगम्य झिल्लियों ;चमतउमंइसम उमउइतंदमद्ध से ढँक कर पूरे बोर्ड को मूल स्थान की मिट्टी से भरे एक पात्र में डुबो कर रख दिया जाता है। इसमें स्थित सूक्ष्मजीव ‘अगर’ के साथ बँॅधे तो होते हैं लेकिन वे पोषक तत्वों, वृद्धिकारकों और प्राकृतिक पर्यावरण से प्राप्त होने वाले सभी तत्वों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं और उनको अवशोषित कर सकते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि जो जीवाणु प्रयोगशाला की सामान्य दशाओ में वृद्धि नहीं कर सकते उन्हें ‘कृत्रिम रूप से उनका नैसर्गिक पर्यावरण’ देकर प्रयोगशाला में वर्धित कर लिया जाता है। इस प्रकार ये वृद्धि न करने वाले जीवाणु भी वृद्धि करने लगते हैं। इस तकनीक का प्रयोग करके लगभग 10ए000 जीवाणुओं को पहचाना जा सका है जो इससे पहले असंवर्धनीय थे । इन्हीं में इलेफ्थेरिया टेरी नामक नया जीवाणु भी प्राप्त हुआ था जिससे टीक्सोबैक्टिन को प्राप्त किया जा सका है। किम लेविस के अनुसार अब हमें ऐसी बहुत सी बातों का पता लग चुका है जो पहले अज्ञात थीं।
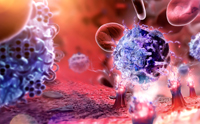 सेण्ट लुइस स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के गौतम डेन्टास कहते हैं - ‘‘सचमुच उपरोक्त तरीका क्रांतिकारी है। इसके फलस्वरूप आज हमें पर्यावरणीय जीवाणुओं के अपेक्षाकृत जितने बड़े वैविध्य को देखने का अवसर मिल रहा है, पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।’’ इन्हीं नए सूक्ष्मजीवों में से शोधदल को एक प्रजाति ऐसी मिली जो स्टैफिलोकोकस ;ैजंचीलसवबवबबनेद्ध नामक जीवाणुओं को प्रभावी तरीके से मार देती है। यह सर्वथा एक नया वंश (जीनस) है और यह एक ऐसे समूह का हिस्सा है जिसका अभी तक प्रतिजैविकों को बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता था। शोधार्थियों ने इसी का नाम इलेफ्थ्ेारिया टेरी ;म्समजिीमतपं जमततंमद्ध रखा। इसमें से टीक्सोबैक्टिन ;ज्मपगवइंबजपदद्ध नामक एक यौगिक निकाला गया जो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों यथा एनथ्रेक्स ;।दजीतंगद्ध और क्षय ;ज्नइमतबनसवेपेद्ध तथा क्लासट्रिडियम डिफिसाइल ;ब्सवेजतमकपनउ कपििपबपसमद्ध (जो गंभीर अतिसार रोग उत्पन्न करता है) जैसे जीवाणुओं को नष्ट कर सकता है ।
सेण्ट लुइस स्थित वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के गौतम डेन्टास कहते हैं - ‘‘सचमुच उपरोक्त तरीका क्रांतिकारी है। इसके फलस्वरूप आज हमें पर्यावरणीय जीवाणुओं के अपेक्षाकृत जितने बड़े वैविध्य को देखने का अवसर मिल रहा है, पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी।’’ इन्हीं नए सूक्ष्मजीवों में से शोधदल को एक प्रजाति ऐसी मिली जो स्टैफिलोकोकस ;ैजंचीलसवबवबबनेद्ध नामक जीवाणुओं को प्रभावी तरीके से मार देती है। यह सर्वथा एक नया वंश (जीनस) है और यह एक ऐसे समूह का हिस्सा है जिसका अभी तक प्रतिजैविकों को बनाने के लिए उपयोग नहीं किया जाता था। शोधार्थियों ने इसी का नाम इलेफ्थ्ेारिया टेरी ;म्समजिीमतपं जमततंमद्ध रखा। इसमें से टीक्सोबैक्टिन ;ज्मपगवइंबजपदद्ध नामक एक यौगिक निकाला गया जो जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोगों यथा एनथ्रेक्स ;।दजीतंगद्ध और क्षय ;ज्नइमतबनसवेपेद्ध तथा क्लासट्रिडियम डिफिसाइल ;ब्सवेजतमकपनउ कपििपबपसमद्ध (जो गंभीर अतिसार रोग उत्पन्न करता है) जैसे जीवाणुओं को नष्ट कर सकता है ।
टीक्सोबैक्टिन को स्टैफिलोकॉकस आरिअस ;ैजंचीलसवबवबबने ंनतपनेद्ध के विरुद्ध अच्छी सक्रियता दिखाने वाले 25 नए यौगिकों में से ढँूॅढ़ निकाला गया था। इसे अब तक का सर्वाधिक संभावनायुक्त यौगिक माना जा रहा है। षोधार्थियों ने सूक्ष्मजीवों को अनेक सप्ताहों तक टीक्सोबैक्टिन के अतिन्यून स्तर पर यह देखने के लिए रखा कि क्या इसमें भी कुछ प्रतिरोधी उपभेद (स्ट्रेन्स) विकसित होते हैं? यह प्रयोग सफल रहा और एक भी प्रतिरोधी उपभेद उत्पन्न नहीं हुआ। यदि आप पूर्ण प्रतिरोध न्यूनता की बात करें तो आमतौर से उसका यह तात्पर्य होता है कि आपने एक इतना विषैला यौगिक ढूॅँढ़ लिया है कि वह मनुष्यों के लिए कभी उपयोगी नहीं होगा। इसीलिए लेविस को बहुत निराशा हुई। किन्तु जब उनके दल के लोगों ने इस औषधि का स्तनपायी जीवों की कोशिकाओं पर प्रयोग किया तो यह बिल्कुल विषैला नहीं था। अब शोधार्थियों को यह नया यौगिक सुरक्षित और कुछ काम का प्रतीत हुआ। यह स्थिर भी रहा और इसमें एक चूहे को एम आर एस ए ;डत्ै।द्ध नामक रसायनप्रतिरोधी स्टैफिलोकोकस के घातक प्रभाव से सुरक्षा प्रदान करने की क्षमता भी देखने को मिली। अब यह शोध धीरे-धीरे आगे बढ़ने लगा । नोवोबायोटिक फार्मास्युटिकल्स के लोसी लिंग और बॉन विश्वविद्यालय के तान्या इडर ने यह दिखा दिया कि टीक्सोबैक्टिन सक्रिय होकर लिपिड प्प् और लिपिड प्प्प् नामक दो अणुओं को प्रतिबाधित कर सकता है। इसमें लिपिड प्प्प् की आवश्यकता जीवाणुओं को अपने चारों ओर की मोटी दीवार या आवरण को बनाने के लिए होती है। लिपिड प्प् जीवाणुओं की इस दीवार को तोड़े जाने से रोकता है। जब जीवाणुओं के निकट टीक्सोबैक्टिन की उपस्थिति होती है तो जीवाणुओं की दीवार ध्वस्त हो जाती है और उसका पुनर्निमाण संभव नहीं होता। यह टीक्सोबैक्टिन रसायन लिपिड प्प् और लिपिड प्प्प् के कुछ अंशों पर चिपक जाता है। यह विभिन्न जीवाणुओं के लिए भी कारगर होता है। जीवाणुओं के लिए टीक्सोबैक्टिन के इस दोहरे आक्रमण से बच सकना संभव नहीं होता।
टीक्सोबैक्टिन अनेक कारणों से अति विशिष्ट और अपनी कार्यशैली में कुछ भिन्न है। यह इस बात से भी सिद्ध होता है कि यह दूसरी ग्लाइकोपेप्टाइड औषधियों जैसे वैन्कोमाइसिन या डैल्बेवैन्सिन से अलग तरीके से सक्रिय होता है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है कि यह एम आर एस ए एन्टेरोकोकाई और क्लासट्रिडियम डिफिसाइल जैसे समस्याप्रद ग्राम पाज़िटिव जीवाणुओं तथा क्षय और एन्थ्रेक्स के जीवाणुओं पर तो प्रभावी है ही यह उसके अतिरिक्त अस्पतालों में संक्रमण का कारण बनने वाले अत्यंत जिद्दी और विपत्तिकारक वी आई एस ए ;टप्ै।द्ध जीवाणुओं को भी समाप्त करने में सहायक हो सकता है। ये संक्रमणकारी जीवाणु सदा से चिकित्सकों के लिए एक भारी सिरदर्द रहे हैं। पूरी आशा है कि टीक्सोबैक्टिन इस प्रतिरोधी जीवाणु को नष्ट करने में पूर्णतः सक्षम होगा। दुर्भाग्यवश टीक्सोबैक्टिन को ग्राम निगेटिव जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावकारी नहीं पाया गया है जैसे कारबेपेनम प्रतिरोधी एनटेरोबैक्टिरिएसी या एन डी एम बग्स जो रोगियों के लिए बड़ा ख़तरा हैं। चूहों पर किए गए परीक्षण में टीक्सोबैक्टिन एमआरएसए, पूतिदोष (सैप्सिस) के उग्र संक्रमणों के तथा फेफड़ों के एस.न्यूमोनी नामक संक्रमण के विरुद्ध अत्यंत शक्तिशाली सिद्ध हुआ है। ‘नेचर’ पत्रिका में इसकी तकनीक की जो व्याख्या प्रकाशित हुई है उसमें भी इसकी क्रियाविधि कुछ जटिल पाई गई हैं। ऐसे संक्रमणों के विरुद्ध टीक्सोबैक्टिन ने शत प्रतिशत सक्रियता प्रदर्शित की है। जिन स्तनपायी जीवों की कोशिकाओं के लिए इनका परीक्षण किया गया उनमें बिलकुल विषालुता नहीं मिली और न रक्त अपक्षयक ;ींमउवसलजपबद्ध सक्रियता ही मिली। इसके कारण डीएनए के जुड़ने की समस्या भी नहीं देखने में आई। अतः शोधार्थी इसके विषय में बहुत आशावान हैं। उन्हें पूर्ण विश्वास है कि टीक्सोबैक्टिन औषधियों के शस्त्रभंडार में एक अत्यन्त घातक और शक्तिशाली अस्त्र सिद्ध होने वाला है। यह औषषि जहॉँ एक ओर चिकित्सालयों में फैलने वाले संक्रमणों के विरुद्ध प्रभावी होगी वहीं हड्डियों या अन्य प्रत्यारोपणों की शल्यक्रिया के बाद की जटिलताओं से भी मुक्ति दिला सकेगी।
 उपरोक्त चर्चा से शायद यह समझा जाना आसान हो जाये कि जीवाणुओं के लिए इस यौगिक के प्रति प्रतिरोध क्षमता विकसित कर पाना कितना दुष्कर है। किन्तु बात प्रत्येक जीवाणु पर लागू नहीं होती। जीवाणुओं में बहुत से जैसे ई.कोलाई, सालमोनेला और हेलिकोबैक्टर में उनकी कोशिका भित्ति के चारों ओर एक और झिल्ली विद्यमान होती है, जो टीक्सोबैक्टिन को वापस कर सकती है। इसी प्रकार की प्रक्रिया इलेफ्थेरिया टेरी ;म्समजिीमतपं जमततंमद्ध नामक जीवाणु भी दर्शा सकता है। ई़.टेरी ही वह सूक्ष्म जीव है जिसका पूर्व में उल्लेख किया गया है और सर्वप्रथम जिसका उपयोग इस औषधि के लिए किया गया है। वास्तव में यह एक विचित्र तथ्य है कि बहुत से प्रतिरोधी उत्परिवर्तन ;डनजंजपवदद्ध जिनके कारण प्रतिजैविक विसरित होते हैं वही उन सूक्ष्मजीवों को उत्पन्न करने के कारण भी बनते हैं जिनसे उन प्रतिजैविकों का जन्म होता है। आखिर उन सूक्ष्मजीवों को भी तो अपनी सुरक्षा का अधिकार है। किन्तु चूंकि ई.टेरी टीक्सोबैक्टिन के प्रति अभेद्य है अतः इसे ऐसे किसी उत्परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आज ऐसा प्रतीत होने लगा है कि यह प्रतिजैविक पूर्णतः प्रतिरोधिता रहित है। इसके पूर्व उपलब्ध प्रतिजैविक वैन्कोमाइसिन ;टंदबवउलबपदद्ध भी लिपिड प्प् से चिपक कर कार्य करता था। यद्यपि यह एक ऐसे अन्य अणु के भाग पर क्रियाशील होता था जो एक सूक्ष्म जीव से दूसरे में होने पर परिवर्तित हो जाता था। अतः जीवाणुओं को इस वैन्कोमाइसिन के लिए प्रतिरोधिता विकसित करने मंे 30 वर्षों का समय लग गया । इस उदाहरण से वैज्ञानिक आशान्वित हैं कि टीक्सोबैक्टिन प्रतिरोधक्षमता प्रदर्शित करने में और अधिक समय भी ले सकता है। इस क्षेत्र में शोधरत अन्य लोगों के अनुसार मानव समाज को निरंतर नए प्रतिजैविकों की जरूरत है। ऐसे प्रतिजैविक जिनकी कार्यप्रणाली में नवीनता हो और जो ज्ञात प्रतिरोधिता की प्रक्रियाओं को हटा सकने की क्षमता रखते हों। अर्थात् ऐसे प्रतिजैविक जो ज्ञात प्रतिरोधक कार्यविन्यास को नियन्त्रित करके उन्हें निष्क्रिय कर सकें। टीक्सोबैक्टिन निश्चित रूप से इस श्रेणी का प्रतिजैविक प्रतीत होता है । इस क्षेत्र में कार्यरत कैरेन बुश (इंडियाना विश्वविद्यालय) का इस विषय में कुछ मतभेद है। उन्हें टीक्सोबैक्टिन की ऐसी अपार प्रतिरोधक क्षमता पर विश्वास नहीं है। उनके अनुसार यह जितना दिखता है उतना प्रतिरोधरोधी नहीं हो सकता। इस प्रकार की प्रतिरोधरोधी क्षमता वाले अन्य कारकों पर भी शोध और विचार किया गया है । यद्यपि उन ओषधियों की उन विशिष्ट परिस्थितियों में कोई प्रतिरोधक्षमता व्यक्त नहीं हो रही थी तथापि अधिक कड़े चुनाव की प्रक्रियाओं में प्रतिरोधी लक्षणों की उपस्थिति दिखने लगी थी। बरमिंघम विश्वविद्यालय से संबद्ध तथा ‘एन्टीबॉयोटिक एक्शन’ की प्रमुख एक सूक्ष्म जीवविज्ञानी लॉरा पिडॉक के विचार में संभव है कि अन्य पर्यावरणीय जीवाणुओं में टीक्सोबैक्टिन के लिए कुछ प्रति उपाय विद्यमान हों । अतः इस बात के प्रति विश्वस्त होना आवश्यक है कि नैदानिक स्थितियों में इस नये प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोधिता विकसित होने की संभावना नहीं है । इसके लिए आवश्यक है कि उसी पर्यावरणीय स्थल से विलग किए गए जीवाणुओं का टीक्सोबैक्टिन प्रतिरोधिता उत्पन्न करने वाले जीनों के लिए भी परीक्षण किया जाए।
उपरोक्त चर्चा से शायद यह समझा जाना आसान हो जाये कि जीवाणुओं के लिए इस यौगिक के प्रति प्रतिरोध क्षमता विकसित कर पाना कितना दुष्कर है। किन्तु बात प्रत्येक जीवाणु पर लागू नहीं होती। जीवाणुओं में बहुत से जैसे ई.कोलाई, सालमोनेला और हेलिकोबैक्टर में उनकी कोशिका भित्ति के चारों ओर एक और झिल्ली विद्यमान होती है, जो टीक्सोबैक्टिन को वापस कर सकती है। इसी प्रकार की प्रक्रिया इलेफ्थेरिया टेरी ;म्समजिीमतपं जमततंमद्ध नामक जीवाणु भी दर्शा सकता है। ई़.टेरी ही वह सूक्ष्म जीव है जिसका पूर्व में उल्लेख किया गया है और सर्वप्रथम जिसका उपयोग इस औषधि के लिए किया गया है। वास्तव में यह एक विचित्र तथ्य है कि बहुत से प्रतिरोधी उत्परिवर्तन ;डनजंजपवदद्ध जिनके कारण प्रतिजैविक विसरित होते हैं वही उन सूक्ष्मजीवों को उत्पन्न करने के कारण भी बनते हैं जिनसे उन प्रतिजैविकों का जन्म होता है। आखिर उन सूक्ष्मजीवों को भी तो अपनी सुरक्षा का अधिकार है। किन्तु चूंकि ई.टेरी टीक्सोबैक्टिन के प्रति अभेद्य है अतः इसे ऐसे किसी उत्परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। आज ऐसा प्रतीत होने लगा है कि यह प्रतिजैविक पूर्णतः प्रतिरोधिता रहित है। इसके पूर्व उपलब्ध प्रतिजैविक वैन्कोमाइसिन ;टंदबवउलबपदद्ध भी लिपिड प्प् से चिपक कर कार्य करता था। यद्यपि यह एक ऐसे अन्य अणु के भाग पर क्रियाशील होता था जो एक सूक्ष्म जीव से दूसरे में होने पर परिवर्तित हो जाता था। अतः जीवाणुओं को इस वैन्कोमाइसिन के लिए प्रतिरोधिता विकसित करने मंे 30 वर्षों का समय लग गया । इस उदाहरण से वैज्ञानिक आशान्वित हैं कि टीक्सोबैक्टिन प्रतिरोधक्षमता प्रदर्शित करने में और अधिक समय भी ले सकता है। इस क्षेत्र में शोधरत अन्य लोगों के अनुसार मानव समाज को निरंतर नए प्रतिजैविकों की जरूरत है। ऐसे प्रतिजैविक जिनकी कार्यप्रणाली में नवीनता हो और जो ज्ञात प्रतिरोधिता की प्रक्रियाओं को हटा सकने की क्षमता रखते हों। अर्थात् ऐसे प्रतिजैविक जो ज्ञात प्रतिरोधक कार्यविन्यास को नियन्त्रित करके उन्हें निष्क्रिय कर सकें। टीक्सोबैक्टिन निश्चित रूप से इस श्रेणी का प्रतिजैविक प्रतीत होता है । इस क्षेत्र में कार्यरत कैरेन बुश (इंडियाना विश्वविद्यालय) का इस विषय में कुछ मतभेद है। उन्हें टीक्सोबैक्टिन की ऐसी अपार प्रतिरोधक क्षमता पर विश्वास नहीं है। उनके अनुसार यह जितना दिखता है उतना प्रतिरोधरोधी नहीं हो सकता। इस प्रकार की प्रतिरोधरोधी क्षमता वाले अन्य कारकों पर भी शोध और विचार किया गया है । यद्यपि उन ओषधियों की उन विशिष्ट परिस्थितियों में कोई प्रतिरोधक्षमता व्यक्त नहीं हो रही थी तथापि अधिक कड़े चुनाव की प्रक्रियाओं में प्रतिरोधी लक्षणों की उपस्थिति दिखने लगी थी। बरमिंघम विश्वविद्यालय से संबद्ध तथा ‘एन्टीबॉयोटिक एक्शन’ की प्रमुख एक सूक्ष्म जीवविज्ञानी लॉरा पिडॉक के विचार में संभव है कि अन्य पर्यावरणीय जीवाणुओं में टीक्सोबैक्टिन के लिए कुछ प्रति उपाय विद्यमान हों । अतः इस बात के प्रति विश्वस्त होना आवश्यक है कि नैदानिक स्थितियों में इस नये प्रतिजैविक के लिए प्रतिरोधिता विकसित होने की संभावना नहीं है । इसके लिए आवश्यक है कि उसी पर्यावरणीय स्थल से विलग किए गए जीवाणुओं का टीक्सोबैक्टिन प्रतिरोधिता उत्पन्न करने वाले जीनों के लिए भी परीक्षण किया जाए।
इसी के समानान्तर लेविस का सहयोगी दल भी परीक्षण कर रहा है। इस दल का उद्देश्य एफडीए ;थ्क्।द्ध से अपनी खोज की स्वीकृति कराना है। यह दल इस बात का प्रयास कर रहा है कि यौगिक के साथ अधिकाधिक खींचतान करके उसे अधिक और अधिक घुलनशील बनाया जा सके जिससे लोगों को उसकी और उच्च मात्रा दी जा सके। अभी वह शोधदल इस बात के लिए भी प्रयासरत है कि आगे भी उस आई चिप ;प बीपचद्ध का उपयोग किया जाए और उससे और अधिक क्षमतावान औषधियॉँ खोजी जा सकें। आज शोधकर्ताओं के समक्ष प्रश्न यह भी है कि क्या हम कभी प्रतिजैविकों के उन पुराने गौरवशाली दिनों को फिर वापस ला सकते हैं?जिस प्रकार टीक्सोबैक्टिन की खोज हुई है और अन्य अधिक सक्षम प्रतिजैविकों की खोज में वैज्ञानिक संलग्न हैं उससे तो यह स्पष्ट है कि हम पुनः प्रतिजैविकों के गौरव को वापस ला सकते हैं। इसमें सन्देह का कोई स्थान नहीं है । ध्यान देने की बात यह है कि प्रयोगशाला में चूहों पर किए गये प्रयोगों से प्रारंभ करके उसे सर्वसुलभ औषधि के रूप में बाजार तक पहुंचाने के मध्य एक लंबी यात्रा है। अभी इस बात का कोई अनुमान नहीं लगाया जा सका है कि यह प्रतिजैविक मानव शरीर पर किसी प्रकार की विषालुता प्रदर्शित करेगा या नहीं?पुराने आँेकड़े बताते है कि प्रयोग शाला में जीवजन्तुओं पर किए गये परीक्षणों में से केवल आठ प्रतिशत ही सक्षम यौगिक के रूप में बाज़ार तक पहँुॅंच पाते है। आज जिस जैविक को ‘प्रतिरोधिता का प्रतिरोधी’ विशेषण से सम्मानित किया जा रहा है वह आगे चलकर अपनी कितनी क्षमता या सक्रियता सिद्ध कर पाता है यह देखने की बात है। फिलहाल अभी तो स्थिति यह है कि अभी हमें इसका उपयोग ‘कृपण के धन’ की तरह करना होगा। इसका कारण यह है कि जब सर्वप्रथम प्रतिजैविकों की खोज हुई तब उसके अत्यंत लाभकारी और जीवनरक्षक गुणों से अति उत्साहित होने के बाद एक ऐसा भी समय आया जब उनका अत्यधिक और मनमाना उपयोग होने लगा। कई देशों में यह चिकित्सक के परामर्श के बिना रोगी की मॉंँग पर सीधे-सीधे दुकानों से खरीदकर खाई जाने वाली औषधि हो गई। इस अबाधित एवं अविवेकपूर्ण उपयोग का परिणाम यह हुआ कि इन प्रतिजैविकों का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा और इन्होंने अनेक स्थितियों के लिए प्रतिरोधिता विकसित कर ली जहाँ पहले यह प्रभावी सिद्ध हेाते थे। वर्तमान समय में स्थिति यह है कि इनकी प्रतिरोधकता के कारण विश्व भर में प्रतिवर्ष 700ए000 लोगों को काल के गाल में समाना पड़ता है। केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही प्रतिवर्ष संक्रमितों की संख्या 2 मिलियन तक पहँुॅच जाती है जिनमें अनुमानित है कि 23ए000 व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। विचारणीय यह है कि आर्थिक दृष्टि से भी प्रतिजैविकों में उपजी प्रतिरोधकता हानिकर सिद्ध होने वाली है। वैज्ञानिक अनुमान लगा रहे हैं कि यदि प्रतिरोध विस्फोट की नौेबत आ गई तो सन् 2050 तक विश्व पर 100 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अतिरिक्त भार बढ़ जाएगा। देशों की सकल घरेलू उत्पाद की दर में भी 2ः से 3ः तक की कमी आने की पूरी आशंका है। आज इसी आशंका के फलस्वरूप पुनः प्रतिजैविकों के विकास की ओर वैज्ञानिक समुदाय उन्मुख हो रहा है। वे लोग केवल इस बात के लिए चिंतित हैं कि जब टीक्सोबैक्टिन बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगा तो कहीं इसके भी ‘अति उपयोग’ से प्रतिरोधकता विकसित होने वाली स्थिति न उत्पन्न हो जाए। यदि इसके उपयोग पर कठोर नियन्त्रण न रखा गया और इसका अति अमूल्य जीवनरक्षक औषधि के रूप में बहुत कृपणता से न इस्तेमाल किया गया तो शायद यह भी बहुत दिनों तक मानवता का साथ न दे सके। टीक्सोबैक्टिन ने हमारी धरती-हमारी मिट्टी-का महत्व एक बार फिर प्रतिष्ठापित कर दिया है क्योंकि यह उसी मिट्टी की उपज है।
mob.no. 09451051033